अपने हस्तिनापुरों में (कविता-संग्रह)
कवयित्री: प्रभा मुजुमदार
प्रकाशक: बोधि प्रकाशन, जयपुर
प्रथम संस्करण: 2014
मूल्य: 100 रु., पृष्ठ संख्या: 148
सत्ता और समाज को आईना दिखाती कविताएँ
राहुल राजेश
हिंदी की सुपरिचित कवयित्री प्रभा मुजुमदार का नया कविता-संग्रह 'अपने हस्तिनापुरों में' मेरे हाथ में है. प्रभा मुजुमदार उन
रचनाकारों में से हैं, जो बिना किसी शोर-शराबे के चुपचाप सृजनरत रहते हैं. यह उनका तीसरा कविता-संग्रह है. इससे पहले उनके दो कविता-संग्रह 'अपने-अपने आकाश' और 'तलाशती हूँ जमीन' क्रमश: प्रकाशित हो चुके हैं. जैसा कि उनके पिछले दोनों संग्रहों के शीर्षकों से भी स्पष्ट है, उनके पहले कविता-संग्रह 'अपने-अपने आकाश' की कविताओं में जहाँ उनका 'निजत्व' मुखर था तो
वहीं उनके दूसरे कविता-संग्रह 'तलाशती हूँ जमीन' की कविताओं में उनका 'स्त्रीत्व' मुखर था. लेकिन अपने तीसरे संग्रह में प्रभा मुजुमदार ने अपने
निजत्व और स्त्रीत्व से आगे बढ़ते हुए, राजनीतिक और सामाजिक विद्रूपताओं को अपना केंद्रीय स्वर बनाया है.
उनके पिछले दो संग्रहों में जहाँ घर-परिवार, समाज में स्त्रियों की स्थिति-नियति और बाजार के फरेब और छलावे सघनता से अभिव्यक्त हुए थे, वहीं उनके इस ताजा संग्रह की लगभग सभी कविताओं में राजीनीति, लोकतंत्र, सत्ता और संपूर्ण समाज में व्याप्त हो गए छल-प्रपंच, साँठ-गाँठ, जोड़-तोड़, उठा-पठक, सुविधापरस्ती, मौकापरस्ती, हिंसा, क्रूरता, षड़यंत्र, धार्मिक असहिष्णुता, प्रायोजित सांप्रादायिकता, अराजकता, दमन-शोषण और अंतत: लोकतंत्र से मोहभंग लेकिन इसके बावजूद हर तरफ पसरी आत्मघाती चुप्पी और संवादहीनता बेहद तीक्ष्णता और उद्विग्नता से अभिव्यक्त हुए हैं.
बोधि प्रकाशन, जयपुर से वर्ष 2014 में बोधि जन-संस्करण के रूप में प्रकाशित इस तीसरे संग्रह 'अपने हस्तिनापुरों में' में कुल अड़सठ कविताएँ हैं. कुछेक कविताओं को छोड़ दें तो लगभग इन सभी कविताओं में मौजूदा समाज और मौजूदा राजनीति में लगातार होते जा रहे पतन और क्षरण के खिलाफ पुरजोर गुस्सा, कटाक्ष और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाने की छटपटाहट बेहद मुखर है. स्वयं प्रभा मुजुमदार अपनी भूमिका में लिखती हैं कि संग्रह की अधिकांश कविताएँ हमारे चारों ओर पसरी संवादहीनता, छीजते हुए मानवीय संबंध, गहराते अवसाद भरे सन्नाटे, अविश्वास, असहिष्णुता एवं क्रूर महत्वाकांक्षाओं की अहंकारी गर्जनाओं के बीच एक अनवरत बेचैनी, छटपटाहट, कुछ करने की व्यग्रता और न कर सकने के अवसाद से गुजरने की प्रक्रिया से उपजी हैं.
सचमुच, आज यह सबसे कड़वा सच है कि संवाद के सारे साधन मौजूद होने और बाजार के तमाम हथकंडों के बावजूद, आज समाज में चुप्पी और संवादहीनता ही समय की सबसे पहली पहचान बन गई है. इसलिए संग्रह की पहली ही कविता का शीर्षक 'संवाद' है जिसमें प्रभा मुजुमदार कहती हैं कि- 'कल तक यहाँ/ संवादों की/ खुली आवाजाही थी/ मगर आज सारे रास्ते/ बंद हो गए हैं.../ अनलिमिटेड टॉकटाइम के बावजूद/ बेधक है यह सन्नाटा.' सबकुछ देखते हुए भी सब, हम सब चुप्प हैं! लेकिन संग्रह की अगली ही कविता में वे इस चुप्पी को बेहद बेबाकी से 'डिकोड' कर देती हैं- 'सब चुप हैं इन दिनों/ और हर एक चुप्पी का/ एक लंबा, गहरा और खामोश अर्थ है.../ मगर यह चुप्पी/ मासूम और बेगुनाह नहीं है/ हवा में एक साजिश की तरह/ घुली है/ और हम सबको/ तमाशबीनों की पंक्ति में/ खड़ा कर चुकी है!' (चुप हैं सब : एक).
लेकिन प्रभा मुजुमदार ने अपनी बेचैनी, आक्रोश और हालात को बयां करने के लिए शब्दों को ही अपना पहला माध्यम बनाया है- 'मेरे लिए/ शब्द एक औजार हैं/ भीतर की टूट-फूट/ उधेड़बुन/ अव्यवस्था और अस्वस्थता की/ शल्यक्रिया के लिए.' इसलिए वे शब्दों की भूमिका को बेहद बारीकी से बयां करती हैं- 'शब्द एक रस्सी की तरह है/ मन के अंधे गहरे कुएँ में/ दफन पड़ी यादों को/ खंगालने के लिए.../ शब्द एक प्रतिध्वनि है/ वीरान, अकेली, निर्वासित नगरी में/ हमसफर की तरह/ साथ चलने के लिए.' (शब्द : एक). लेकिन वह इसी संग्रह की भूमिका में यह भी रेखांकित करती हैं कि शब्द की सत्ता और महत्ता, इन दिनों या तो
नेपथ्य में मौन साधे खड़ी है अथवा बाजार की चकाचौंध में अपनी उपयोगिता तलाश रही है
और सत्ता के हर मठ और गढ़ के आगे अपने को नवाजे जाने की कवायद भी कर रही है. इसलिए वह
अपनी कविता में लिखती हैं-
'शब्द अब/ बिकने लगे हैं मंडियों में/ उत्पाद बनकर/ और बिचौलियों के समूह/ आ खड़े होते हैं/ उनके दाम आंकने के लिए/ अपने-अपने लेबल/ और पैकिंग के साथ.' (शब्द : तीन).
लेकिन विश्वसनीयता
के इस गहराते संकट के बीच,
उन्हें यह पूरा विश्वास है कि सारी विद्रूपताओं, विषमताओं और छद्म-छलावों के बावजूद सत्य और मनुष्यता की जड़ें अब भी जिंदा हैं क्योंकि- 'जड़ें जानती हैं/ अपने को जिंदा रखना/ अंधेरे और गुमनामी के/ बरसों, सदियों, युगों में भी.' (जड़ें जिंदा हैं : एक). इसलिए वे पूरे विश्वास के साथ कहती हैं- 'सुलगते हुए जंगल में/ बाकी होंगी ही कई जड़ें/ बारिश के इंतजार में/ लहलहाने को तैयार.' (जड़ें जिंदा हैं : तीन).
आज के दौर में
समय की रफ्तार बहुत बढ़ गई है, सूचना-क्रांति अपने चरम पर पहुँचकर विकाराल और विध्वसंक हो गई है और
आक्रामक बाजार की चपेट हर कोई आ गया है. फलत: आदमी संवेदनाशून्य
हो गया है और आदमी की आदमियत ही दाँव पर लग गई है. इसलिए प्रभा मुजुमदार महसूस करती
हैं कि- 'इन दिनों/ किसी की खुशी पर/ नहीं होती खुशी/ और न ही छू पाती
है/ किसी की कोई पीड़ा.../ किसी की मदद के
लिए/ उठने से पहले हाथ,/ सोचने लगता है
दिमाग/ नफे-नुकसान का हिसाब.' (इन दिनों : एक). ऐसी परिस्थिति
में मनुष्य का पूरा वजूद ही किसी और की गिरफ्त में आ गया है और मनुष्य की हरेक गतिविधि
का संचालन अब किसी और के हाथों हो रहा है. इसलिए वे लिखती हैं- 'मैं एक प्यादा/ शतरंज की बिसात
पर/ बिछाया हुआ/ शहादत के लिए.../ मैं एक नागरिक/ आँकड़ों के मोहक
जाल में/ बहलाए जाने के लिए.../ मैं एक वोटर/ वक्त-बेवक्त के
चुनावों के लिए!' (वजूद).
प्रभा मुजुमदार
ईश्वर और धर्म के नाम पर चल रहे कर्म-कांड, स्वांग और अभियान
को भी ईश्वर की मौत ही मानती हैं. इसलिए वे लिखती हैं- 'कहते हैं/ ईश्वर मर गया है/ क्या सच?/ फिर कौन है/ उसका उत्तराधिकारी?/ या उत्तराधिकार
की ही/ लड़ाई लड़ रहे हैं/ इतने सारे शैतान?' (ईश्वर की मौत पर). इसी तरह वे सतयुग
के बहुप्रचारित दावों और स्थापित सत्यों पर भी संदेह करती हैं और उसका तार्किक विश्लेषण
करती हैं. 'सतयुग में जीने से' कविता में वे कहती
हैं- 'जितने भी संकेत/ और पुरावे मिलते
हैं,/ काफी हैं मोहभंग के लिए/ सच और झूठ की/ पहचान के लिए/ क्योंकि तब भी
रूप बदलकर किए जाते थे/ हत्याएँ और बलात्कार/ याचक का भेष धरकर/ हथिया ली जाती
थी संपदा/ छल से जीता जाता था बल/ रिश्तों में सेंध
लगाकर/ छीनी जाती थी सिद्धि.' इसलिए कविता के
अंत में वे पाती हैं कि- 'शायद हम बेहतर हैं/ इस युग में ही/ अपने दुख, दुविधाओं और/ तमाम असुरक्षाओं
के बावजूद.'
अपनी कविताओं में
वे समाज में व्याप्त दोगलेपन और हर मोड़ पर गाल बजा रहे विदूषकों की भी स्पष्ट पहचान
करती हैं- 'वही लोग/ जिन्होंने भ्रष्टाचार
के विरोध में/ आसमान उठा रखा था सिर पर/ अपने और अपनों
को बचाने के लिए आज/ समझौते की संभावनाएँ ढूढ़
रहे हैं.../ माफिया और अपराधियों के/ विरोध में/ जन आंदोलन खड़ा
करने वालों की/ अलमारियों के भीतर से/ गिर रहे हैं नर-कंकाल.' (विदूषकों के बीच). लेकिन उन्हें
मालूम है कि यहाँ इतनी आसानी से कुछ भी नहीं बदलने वाला, क्योंकि यहाँ हर
चीज पहले से ही तय और प्रायोजित है, क्योंकि यहाँ हरबार 'उन्हीं की चौसर/ उन्हीं का खेल/ उन्हीं की गोटी/ उन्हीं के दाँव/ उन्हीं के दर्शक/ उन्हीं के समर्थक/ आयोजक/ निर्णायक' (हर बार : तीन) होते हैं और हम
हर बार वही इतिहास दुहराने को विवश होते हैं.
इस संग्रह में
गौर करने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभा मुजुमदार राजनीति, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र जैसे शब्दों
के मौजूदा फरेब को बखूबी पहचानती हैं और संग्रह की तमाम कविताओं में उन्हें भरसक उजागर
करने का प्रयास करती हैं. इसके लिए वे मिथकों और महाभारत के दृष्टांतों का सारगर्भित
इस्तेमाल भी करती हैं. यही कारण है कि उन्होंने इस संग्रह का नाम भी 'अपने हस्तिनापुरों
में' रखा है, जो इस संग्रह के केंद्रीय स्वर को मुखरता से प्रतिध्वनित करता
है. उन्होंने संग्रह की संक्षिप्त भूमिका में लिखा भी है कि हस्तिनापुर सत्ता का स्थायी
प्रतीक है. इसलिए महलों-दरबारों में चली जा रही शतरंजी चालें, ईर्ष्या, ब्लैकमेलिंग, नैतिकता की सुविधानुसार
व्याख्या, अवसर के अनुरूप चुप्पी और वक्तव्य, लालसाओं का विस्फोट, येनकेन-प्रकारेन कार्यसिद्धि, हिंसा और विध्वंस
द्वारा अर्जित विजय के बाद की अराजकता, अनिश्चितता, मोहभंग और विरक्ति
भी हरेक देश-काल में सत्ता-केंद्रों के इर्दगिर्द घटित होने वाली कमोबेश
स्थायी प्रवृतियाँ ही हैं.
संग्रह में 'अपने हस्तिनापुरों
में' शीर्षक से छह कविताएँ हैं जो सत्ता से जुड़ी इन प्रवृतियों का
बहुत सटीक चित्रण करती हैं. इस श्रृंखला की पहली कविता की शुरूआत में ही हमें सत्ता
की सुविधापरस्ती की साफ झलक देखने को मिल जाती है- 'धृतराष्ट्र होने
का मतलब/ अंधा होना नहीं होता./ धृतराष्ट्र होना
होता है,/ अपनी मर्जी, खुशी और/ सुविधा के साथ,/ कुछ भी देख सकने
की दिव्यदृष्टि./ कुछ भी अनदेखा/ कर सकने की आजादी.' सत्ता की मौकापरस्ती
भी इस श्रृंखला की दूसरी कविता बखूबी बयां कर देती है- ''क' के खिलाफ हैं/ पंचानबे मुकदमे/ 'ख' के खाते में दर्ज
हैं सौ./ 'ग' ने ताउम्र/ जेल से खेली है
राजनीति./ एक का वोट बंधा/ जाति के नाम,/ तो दूसरे ने काटी
है/ धर्म की फसल./ और यह तीसरा,/ बाँट रहा है सबको/ भाषाओं के नाम./ ...वे तीनों आश्वस्त
हैं/ अपनी चाल के/ तुरूप के पत्ते
से./ ...उन्हीं में से तो आएगा कोई,/ ढोल धमाकों के
साथ/ हमारा भाग्य विधाता बन.'
इस श्रृंखला की
पाँचवी कविता जनतंत्र की मौजूदा सच्चाई को एकबारगी बेपरदा कर देती है और आज के लोकतंत्र
के बारे में कुछ कहने को बाकी नहीं रह जाता- 'जनतंत्र,/ जन की नहीं/ धन की शक्ति से
चलता है./ जैसे हर भगवान को चाहिए,/ विराट और समृद्ध
मंदिर/ भेंट और चढ़ावे/ सुरक्षा और दिव्यत्व/ भक्त और महंत./ जनतंत्र को भी
चाहिए रुतबा./ अभेद्य सुरक्षाचक्र से मंडित,/ संसद, विधानसभाएँ/ मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति के
लिए,/ आलीशान कोठियाँ, महल, बगीचे./ वर्दी और मैडल
से सुसज्जित कमांडो,/ लालबत्ती, सायरन, लंबे काफिले,/ वेतन, भत्ते, सुविधाएँ,/ विदेश यात्राएँ, विशेष विमान,/ फूल-मालाएँ, चढ़ावे./ प्रवचन सुनने,/ तालियाँ बजाने
को तत्पर/ भक्तों की जमात.' इसी कविता में
आगे वे लोकतंत्र के महापर्व यानी मतदान का सच भी कटाक्षपूर्वक सामने रख देती हैं- 'एक वोट डालने से
नहीं हिलती/ दिल्ली की सल्तनत/ यूँ दिल बहलाने
के लिए/ अच्छा ख्याल है यह भी!'
लेकिन इस श्रृंखला
की अंतिम कविता यानी 'अपने हस्तिनापुरों में : छह' में प्रभा मुजुमदार
जनतंत्र के इस पतन के लिए हमें भी जिम्मेदार ठहराती हैं- 'कैद हैं हम/ अपने हस्तिनापुरों
में/ बगैर जंजीरों के/ कारागार के दीवारों
के बाहर./ समर्थ, चेतन,/ विवेकवान होने
के बावजूद,/ देख रहे हैं,/ मनुष्यत्व के विरोध
में/ षड़यंत्रों का अंतहीन सिलसिला./... जानते हुए भी कि/ बस एक आवाज भर
शेष है/ तमाम मुर्दों में प्राण फूँकने के लिए/ फिर भी मुँह से
नहीं निकलती/ बगावत की आवाज.' इसलिए वे इस कविता-श्रृंखला के अंत
में हमसे सीधे सवाल करती हैं- 'कौन-सा वह मोह है?/ किस बात का इंतजार
है?/ कौन-सी वे प्रतिज्ञाएँ/ तन, मन, मस्तिष्क को जकड़े
हुए/ पत्थर-सी लदी सीने पर?/ क्या हम/ अपने आप से मुक्त
नहीं हो सकते?' लेकिन सच तो यह है कि हम
तभी मुक्त हो सकेंगे, जब हम अपने निजी और क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर उठेंगे और निजहित
से पहले देशहित के बारे में सोचेंगे!
इस संग्रह में
इसी तेवर और मिजाज की कई अन्य कविताएँ भी हैं. लेकिन वे सब की सब व्यग्रता और बेचैनी
की एक जैसी मन:स्थिति में ही रची जान पड़ती हैं. इसलिए उनमें एक ही विषय का
सायास दुहराव और कमोबेश सपाटबयानी दिखती है. यही कारण है कि संग्रह की ऐसी अनेक कविताएँ
अनावश्यक विस्तार और अवांछित दुहराव का शिकार हो गई हैं, जो कविताओं की
सतत पठनीयता को बाधित भी करती हैं. संग्रह में अनेक कविताओं का एक, दो, तीन, चार,
पाँच खंडों तक जबरन विस्तार भी खटकता है. लेकिन इसके बावजूद, संग्रह में 'जंगली घास', 'एक मामूली आदमी', 'अपने तहखाने में', 'वक्त मिलने पर', 'दामिनी-सी', 'बच्चों के आने
पर', 'उम्मीद है', 'संभावना' और 'जिंदगी हूँ मैं' कुछ ऐसी कविताएँ
हैं, जिसमें कवयित्री का निजत्व, मनुष्य की सकारात्मक ऊर्जा, उमंग, उत्साह और जिंदगी
की रवानियत प्रतिध्वनित होती हैं और हमें समाज, सत्ता और राजनीति
की कड़वी सच्चाइयों से थोड़ी राहत मिलती है.
मुझे इस संग्रह
में निजी तौर जो कविताएँ सबसे अधिक पसंद आईं, उनमें से एक है- 'बच्चों के आने
पर'. इस कविता की पंक्तियाँ मन को छू लेती हैं- 'फिर फुदकने लगी
चिड़िया/ आँगन में./ फूलों से भर गई
बगिया./ महकने लगी हवा./ उतर आया बसंत/ चुपके से आँगन
में./ ...एक अरसे बाद,/ जान आ गई रसोईघर
में/ खुशबू, रंग और स्वाद से./ घनघनाने लगे सारे
फोन/ देर रात तक.' इतना ही नहीं, बच्चों के घर आने
पर खुद घर भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि- 'घर का एक कोना/ पहचानता है तुम्हें/ मेरे बच्चो!/ तुम्हारी खिलखिलाहट,/ झूठ, प्यार और शरारत,/ डर और आँसू,/ सपनों और चाहतों
को,/ वैसे ही समेट रखा है इसने अपने भीतर.' इसी तरह 'उम्मीद है' शीर्षक कविता की
शुरुआती पंक्तियाँ भी मुझे बाँध लेती हैं- 'जब तक/ एक पत्ता भी/ खड़कता है अंधेरे
में,/ सन्नाटे को/ मिल रही है चुनौती.' संग्रह की अंतिम
कविता 'जिंदगी हूँ मैं' भी हमारी सारी
हताशा-निराशा हर लेती है और हममें फिर से जीने की ताकत भर देती है- 'फिर फिर लौटकर/ दस्तक देती रहूँगी
मैं,/ तुम्हारे बंद दरवाजे पर./ ...जिंदगी हूँ मैं./ मौत की तमाम/ वेदना और हाहाकार
के बीच,/ छुपा रखूँगी/ अपने कुछ अंकुर.'
कुल मिलाकर, प्रभा मुजुमदार
का यह तीसरा संग्रह 'अपने हस्तिनापुरों में' पठनीय और
सराहनीय है. उम्मीद करता हूँ कि प्रभा मुजुमदार अपना अगला संग्रह निकालने से पहले
थोड़ा ठहरेंगी, अपनी कविताओं को और कसेंगी, उन्हें और पकने
देंगी और अभिव्यक्ति की सघन रचनात्मक बेचैनी के बावजूद किसी भी हड़बड़ी से बचेंगी.
संग्रह में प्रूफ की कुछ गलतियाँ रह गई हैं, लेकिन वे कविता
के आस्वाद में ज्यादा विघ्न नहीं डालतीं. हाँ, मुझे पता नहीं
क्यों इस संग्रह का नाम कुछ खटकता रहा और मैं इसे 'अपने हस्तिनापुरों
में' की बजाय, हर बार 'अपने-अपने हस्तिनापुर
में' ही पढ़ता रहा!
राहुल राजेश
सहायक प्रबंधक (राजभाषा), भारतीय रिज़र्व बैंक, मुख्य कार्यालय भवन,
आश्रम रोड, अहमदाबाद-380014 (गुजरात).
मो. 09429608159, rahulrajesh2006@gmail.com
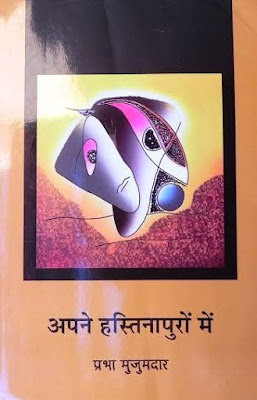

आपकी इस प्रविष्टि् के लिंक की चर्चा कल रविवार (08-11-2015) को "अच्छे दिन दिखला दो बाबू" (चर्चा अंक 2154) (चर्चा अंक 2153) पर भी होगी।
जवाब देंहटाएं--
सूचना देने का उद्देश्य है कि यदि किसी रचनाकार की प्रविष्टि का लिंक किसी स्थान पर लगाया जाये तो उसकी सूचना देना व्यवस्थापक का नैतिक कर्तव्य होता है।
--
चर्चा मंच पर पूरी पोस्ट नहीं दी जाती है बल्कि आपकी पोस्ट का लिंक या लिंक के साथ पोस्ट का महत्वपूर्ण अंश दिया जाता है।
जिससे कि पाठक उत्सुकता के साथ आपके ब्लॉग पर आपकी पूरी पोस्ट पढ़ने के लिए जाये।
हार्दिक शुभकामनाओं के साथ।
सादर...!
डॉ.रूपचन्द्र शास्त्री 'मयंक'
बहुत सुंदर रचना।
जवाब देंहटाएंNice information
जवाब देंहटाएंएक टिप्पणी भेजें
आप अपनी प्रतिक्रिया devarun72@gmail.com पर सीधे भी भेज सकते हैं.